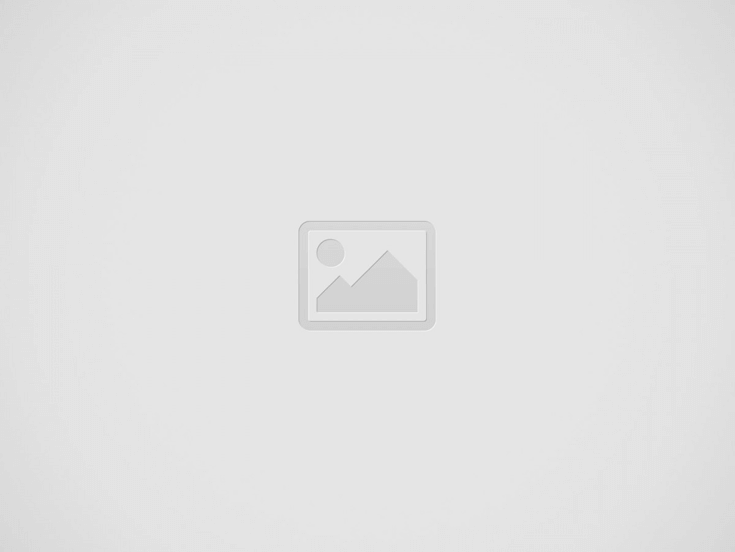

कांग्रेस समर्थक सिद्ध शर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने एक तस्वीर ट्वीट की है। तस्वीर एक स्लम इलाके की है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, “कभी देखा है #विकास?? विकास को करीब से देखें और बताएं कि वह आपको कैसा लगता है!!!”
असल में इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर इसमें एक व्यक्ति का चेहरा दिखता है। इस पोस्ट को डेढ़ हजार लोगों ने लाइक किया है। वहीं लगभग 400 लोग इसे रिपोस्ट कर चुके हैं, पोस्ट के कमेंट सेक्शन में जायदा तरह लोग इसे भारत से जोड़कर देख रहे है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सच में यह मलिन बस्ती भारत में है? चलिए इस दावे की पड़ताल करते हैं।
यह भी पढ़े: योगी आदित्यनाथ ने रविवार का साप्ताहिक अवकाश को निरस्त नहीं किया है; ट्विटर यूजर ने फैलाई भ्रांतियां
इस तस्वीर के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमने ‘गूगल रिवर्स इमेज’ सर्च की मदद से इसे इंटरनेट पर ढूंढा। इस दौरान यह तस्वीर हमें ‘9GAG‘ नाम की एक वेबसाइट पर मिली, जिसके कैप्शन में लिखा था “The third world sometimes is art”
इसमें कहीं भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह तस्वीर कहां की है और इसमें कौन है, लेकिन इसके कमेंट सेक्शन में हमें इस बात का सुराग मिला कि यह तस्वीर किसकी है। एक यूजर ने इस तस्वीर में दिख रहे शख्स की असल इमेज पोस्ट की है।
यह जब हमने इस फोटो को रिवर्स इमेज की मदद से सर्च किया तो पता चला कि यह ब्राजील के राष्ट्रपति “लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा” हैं।
वहीं कई 9GAG वेबसाइट पर ब्राज़ील नाम के अकाउंट से यही तस्वीर पोस्ट की गई है, जिससे यह पक्का होता है कि यह स्लम इलाके की तस्वीर भी ब्राज़ील की है।
हमारी पड़ताल में आगे यही फोटो एक c. alster नाम के ट्विटर अकाउंट पर मिली। कैप्शन में लिखा है “आप एक अपराधी से क्या उम्मीद करते हैं? गरीबी बद से बदतर होती जा रही है। ब्राज़ील की हालत इतनी जल्दी कैसे ख़राब हो सकती है?”
हमारी पड़ताल में यह स्पष्ट हो गया कि ट्वविटर यूजर द्वारा पोस्ट की गई यह तस्वीर ब्राज़ील की है। ऊपर उल्लेख किए गए तमाम प्रमाण के आधार पर यह कहना उचित होगा कि भारत का बताकर शेयर की जा रही यह तस्वीर झूठी है।
| दावा | स्लम इलाके की तस्वीर को सोशल मीडिया उसर भारत से जोड़ रहे है। |
| दावेदार | ट्वीटर यूजर |
| फैक्ट चेक | झूठा |
प्रिय पाठकों, हम भारत के खिलाफ फर्जी खबरों को उजागर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारे पास अन्य लोगों की तरह कोई कॉर्पोरेट फंडिंग नहीं है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और आगे बढ़ने में मदद करेगा। आप हमें लिविक्स मीडिया फाउंडेशन क्यूआर कोड द्वारा भी सहयोग कर सकते हैं।
This website uses cookies.